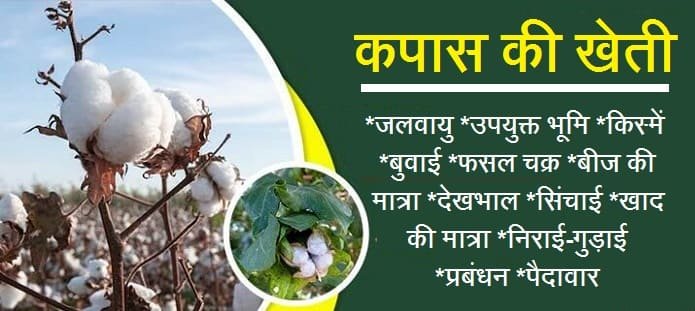
कपास की खेती भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशा और नगदी फसल में से एक है| और देश की औदधोगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है| कपास की खेती लगभग पुरे विश्व में उगाई जाती है| यह कपास की खेती वस्त्र उद्धोग को बुनियादी कच्चा माल प्रदान करता है| भारत में कपास की खेती लगभग 6 मिलियन किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर आजीविका प्रदान करता है और 40 से 50 लाख लोग इसके व्यापार या प्रसंस्करण में कार्यरत है|
व्यावसायिक रूप से कपास की खेती को सफेद सोना के रूप में भी जाना जाता है| देश में व्यापक स्तर पर कपास उत्पादन की आवश्यकता है| क्योंकी कपास का महत्व इन कार्यो से लगाया जा सकता है इसे कपड़े बनते है, इसका तेल निकलता है और इसका विनोला बिना रेशा का पशु आहर में व्यापक तौर पर उपयोग में लाया जाता है|
लम्बे रेशा वाले कपास को सर्वोतम माना जाता है जिसकी लम्बाई 5 सेंटीमीटर इसको उच्च कोटि की वस्तुओं में शामिल किया जाता है| मध्य रेशा वाला कपास (Cotton) जिसकी लम्बाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर होती है इसको मिश्रित कपास कहा जाता है| तीसरे प्रकार का कपास छोटे रेशा वाला होता है| जिसकी लम्बाई 3.5 सेंटीमीटर होती है|
यह भी पढ़ें- बीटी कपास की खेती कैसे करें: किस्में, देखभाल और पैदावार
कपास की खेती के लिए जलवायु
कपास की उत्तम फसल के लिए आदर्श जलवायु का होना आवश्यक है| फसल के उगने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेट और अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेट होना उचित है| इसकी बढ़वार के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए| फलन लगते समय दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेट तथा रातें ठंडी होनी चाहिए| कपास के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है| 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना हानिकारक होता है|
कपास की खेती के लिए भूमि
कपास के लिए उपयुक्त भूमि में अच्छी जलधारण और जल निकास क्षमता होनी चाहिए| जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहां इसकी खेती अधिक जल-धारण क्षमता वाली मटियार भूमि में की जाती है| जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों वहां बलुई एवं बलुई दोमट मिटटी में इसकी खेती की जा सकती है| यह हल्की अम्लीय एवं क्षारीय भूमि में उगाई जा सकती है| इसके लिए उपयुक्त पी एच मान 5.5 से 6.0 है| हालाँकि इसकी खेती 8.5 पी एच मान तक वाली भूमि में भी की जा सकती है|
कपास की खेती और फसल चक्र
जलवायु, भूमि, सिंचाई की सुविधाओं तथा किसानों की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार कपास की फसल भिन्न-भिन्न फसल चक्र के अंतर्गत उगाई जा सकती है जो इस प्रकार से हैं, जैसे-
वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए फसल चक्र-
मध्य और दक्षिण भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों में कपास की एक ही फसल उगाई जाती है| कपास के बाद अगले वर्ष बाजरा, ज्वार या मिर्च आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं|
सिंचाई आधारित क्षेत्रों के लिए फसल चक्र-
1. कपास- गेहूं या जौ
2. कपास – बरसीम या सेंजी या जई
3. कपास – सूरजमुखी
4. कपास – मूंगफली कपास आदि|
यह भी पढ़ें- देसी कपास की खेती कैसे करें: किस्में, देखभाल और पैदावार
कपास और अन्र्तफसली खेती
कपास की कतारों के बीच एक कतार बैसाखी मूंग की बोना लाभप्रद है| बारानी क्षेत्र में अन्तर्शस्य अपनाना उपयुक्त है, जुड़वा कतार विधि से अन्तर्शस्य अधिक लाभप्रद रहती है| सिंचित क्षेत्र में निम्न फसल चक्र लाभप्रद एवं उपज में वृद्धि करने वाले पाये गये हैं, जैसे-
1. कपास – गेहूं या मटर (एक वर्ष)
2. मक्का – गेहूं – कपास – मैथी (दो वर्ष)
3. मक्का – सरसों – कपास – मैथी (दो वर्ष)
4. ग्वार – गेहूं – चारा – कपास (दो वर्ष)
उत्तरी भारत में कपास- गेहूं, कपास – मटर एवं कपास – ज्वार और दक्षिणी भारत में कपास – धान, कपास – ज्वार, कपास – मूंगफली एवं धान – कपास फसल चक्र मुख्य हैं| उत्तरी भारत में कपास के बाद गेहूं की फसल लेने के लिए कपास की जल्दी पकने वाली किस्में बोनी चाहिए एवं गेहूं की देर से बोने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए|
हाल ही में हुए अनुसंधान से पता चला है, कि कपास की कटाई के बाद बिना जुताई आधुनिक मशीनों के द्वारा गेहूं की समय पर बुवाई की जा सकती है| जिससे अधिक उपज और पानी की बचत होती है| बिना जुताई के खेती कपास – गेहूं फसल चक्र में ज्यादा सटीक सिद्ध हुई है|
यह भी पढ़ें- नरमा (अमेरिकन) कपास की खेती कैसे करें
कपास की उन्नत किस्में
किसान भाइयों वर्तमान में बी टी कपास का बोलबाला है| जिसकी किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र, परिस्थितियों और क्षेत्र की प्रचलित किस्म के अनुसार ही करें| लेकिन कुछ प्रमुख नरमा, देशी और संकर कपास की अनुमोदित किस्में क्षेत्रवार इस प्रकार है, जैसे-
उत्तरी क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में-
| राज्य | नरमा (अमरीकन) कपास | देशी कपास | संकर कपास |
| पंजाब | एफ- 286, एल एस- 886, एफ- 414, एफ- 846, एफ- 1861, एल एच- 1556, पूसा- 8-6, एफ- 1378 | एल डी- 230, एल डी- 327, एल डी- 491, पी एयू- 626, मोती, एल डी- 694 | फतेह, एल डी एच- 11, एल एच एच- 144 |
| हरियाणा | एच- 1117, एच एस- 45, एच एस- 6, एच- 1098, पूसा 8-6 | डी एस- 1, डी एस- 5, एच- 107, एच डी- 123 | धनलक्ष्मी, एच एच एच- 223, सी एस ए ए- 2, उमा शंकर |
| राजस्थान | गंगानगर अगेती, बीकानेरी नरमा, आर एस- 875, पूसा 8 व 6, आर एस- 2013 | आर जी- 8 | राज एच एच- 116 (मरू विकास) |
| पश्चिमी उत्तर प्रदेश | विकास | लोहित यामली | – |
मध्य क्षेत्र हेतु अनुमोदित किस्में-
| राज्य | नरमा (अमेरिकन) कपास | देशी | संकर |
| मध्य प्रदेश | कंडवा- 3, के सी- 94-2 | माल्जरी | जे के एच वाई 1, जे के एच वाई 2 |
| महाराष्ट्र | पी के वी- 081, एल आर के- 516, सी एन एच- 36, रजत | पी ए- 183, ए के ए- 4, रोहिणी | एन एच एच- 44, एच एच वी- 12 |
| गुजरात | गुजरात कॉटन- 12, गुजरात कॉटन- 14, गुजरात कॉटन- 16, एल आर के- 516, सी एन एच- 36 | गुजरात कॉटन 15, गुजरात कॉटन 11 | एच- 8, डी एच- 7, एच- 10, डी एच- 5 |
यह भी पढ़ें- धान की खेती: जलवायु, किस्में, देखभाल और पैदावार
दक्षिण क्षेत्र हेतु अनुमोदित किस्में-
| राज्य | नरमा (अमेरिकन) कपास | देशी | संकर |
| आंध्र प्रदेश | एल आर ए- 5166, एल ए- 920, कंचन | श्रीसाईंलम महानदी, एन ए- 1315 | सविता, एच बी- 224 |
| कर्नाटक | शारदा, जे के- 119, अबदीता | जी- 22, ए के- 235 | डी सी एच- 32, डी एच बी- 105, डी डी एच- 2, डी डी एच- 11 |
| तमिलनाडु | एम सी यू- 5, एम सी यू- 7, एम सी यू- 9, सुरभि | के- 10, के- 11 | सविता, सूर्या, एच बी- 224, आर सी एच- 2, डी सी एच- 32 |
पिछले 10 से 12 वर्षों में बी टी कपास की कई किस्में भारत के सभी क्षेत्रों में उगाई जाने लगी हैं| जिनमें मुख्य किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे- आर सी एच- 308, आर सी एच- 314, आर सी एच- 134, आर सी एच- 317, एम आर सी- 6301, एम आर सी- 6304 आदि है|
कपास की खेती के लिए खेत की तैयारी
दक्षिण व मध्य भारत में कपास वर्षा-आधारित काली भूमि में उगाई जाती है| इन क्षेत्रों में खेत तैयार करने के लिए एक गहरी जुताई मिटटी पलटने वाले हल से रबी फसल की कटाई के बाद करनी चाहिए, जिसमें खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और वर्षा जल का संचय अधिक होता है| इसके बाद 3 से 4 बार हैरो चलाना काफी होता है| बुवाई से पहले खेत में पाटा लगाते हैं, ताकि खेत समतल हो जाए| उत्तरी भारत में कपास की खेती मुख्यतः सिंचाई आधारित होती है|
इन क्षेत्रों में खेत की तैयारी के लिए एक सिंचाई कर 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए एवं इसके बाद 3 से 4 हल्की जुताई कर, पाटा लगाकर बुवाई करनी चाहिए| कपास का खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत पूर्णतया समतल हो ताकि मिटटी की जलधारण एवं जलनिकास क्षमता दोनों अच्छे हों| यदि खेतों में खरपतवारों की ज्यादा समस्या न हो तो बिना जुताई या न्यूनतम जुताई से भी कपास की खेती की जा सकती है|
यह भी पढ़ें- कपास की जैविक खेती: किस्में, देखभाल और पैदावार
कपास की खेती के लिए बीज की मात्रा
संकर तथा बी.टी. के लिए चार किलो प्रमाणित बीज प्रति हैक्टेयर डालना चाहिए| देशी और नरमा किस्मों की बुवाई के लिए 12 से 16 किलोग्राम प्रमाणित बीज प्रति हैक्टेयर की दर से प्रयोग करें| बीज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें|
कपास की खेती के लिए बीज उपचार
1. कपास के बीज में छुपी हुई गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिये बीजों को धूमित कर लीजिये| 40 किलोग्राम तक बीज को धूमित करने के लिये एल्यूमीनियम फॉस्फॉइड की एक गोली बीज में डालकर उसे हवा रोधी बनाकर चौबीस घण्टे तक बन्द रखें| धूमित करना सम्भव न हो तो तेज धूप में बीजों को पतली तह के रूप में फैलाकर 6 घण्टे तक तपने देवें|
2. बीजों से रेशे हटाने के लिये जहां सम्भव हो, 10 किलोग्राम बीज के लिये एक लीटर व्यापारिक गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है| मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में बीज डालकर तेजाब डालिये तथा एक दो मिनट तक लकड़ी से हिलाईये| बीज काला पड़ते ही तुरन्त बीज को बहते हुए पानी में धो डालिये एवं ऊपर तैरते हुए बीज को अलग कर दीजिये| गंधक के तेजाब से बीज के उपचार से अंकुरण अच्छा होगा| यह उपचार कर लेने पर बीज को प्रधूमन की आवश्यकता नहीं रहेगी|
3. बीज जनित रोग से बचने के लिये बीज को 10 लीटर पानी में एक ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या ढाई ग्राम एग्रीमाइसिन के घोल में 8 से 10 घण्टे तक भिगोकर सुखा लीजिये इसके बाद बोने के काम में लेवें|
4. जहाँ पर जड़ गलन रोग का प्रकोप होता है ट्राइकोड़मा हारजेनियम या सूडोमोनास फ्लूरोसेन्स जीव नियन्त्रक से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या रासायनिक फफूंदनाशी जैसे कार्बोक्सिन 70 डब्ल्यू पी, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या कार्बेन्डेजिम 50 डब्ल्यू पी से 2 ग्राम या थाईरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें|
5. रेशे रहित एक किलोग्राम नरमे के बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 डब्ल्यू एस या 4 ग्राम थायोमिथोक्साम 70 डब्ल्यू एस से उपचारित कर पत्ती रस चूसक हानिकारक कीट और पत्ती मरोड़ वायरस को कम किया जा सकता है|
6. असिंचित स्थितियों में कपास की बुवाई के लिये प्रति किलोग्राम बीज को 10 ग्राम एजेक्टोबेक्टर कल्चर से उपचारित कर बोने से पैदावार में वृद्धि होती है|
यह भी पढ़ें- संकर धान की खेती कैसे करें: किस्में, देखभाल और पैदावार
कपास की बुवाई का समय तथा विधि
1. कपास की बुवाई का उपयुक्त समय अप्रेल के द्वितीय पखवाड़े से मई के प्रथम सप्ताह तक है|
2. अमेरिकन किस्मों की कतार से कतार की दूरी 60 सेन्टीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेन्टीमीटर रखनी चाहिये|
3. देशी किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेन्टीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेन्टीमीटर रखनी चाहिये|
4. बी टी कपास की बुवाई बीज रोपकर (डिबलिंग) 108 X 60 सेंटीमीटर अर्थात 108 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे 60 सेंटीमीटर या 67.5 X 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करें|
5. पौलीथीन की थैलियों में पौध तैयार कर रिक्त स्थानों पर रोप कर वांछित पौधों की संख्या बनाये रख सकते हैं|
6. लवणीय भूमि में यदि कपास बोई जाये तो मेड़े बनाकर मेड़ों की ढाल पर बीज उगाना चाहिए|
कपास में खाद एवं उर्वरक की मात्रा
1. बुवाई से तीन चार सप्ताह पहले 25 से 30 गाड़ी गोबर की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से जुताई कर भूमि में अच्छी तरह मिला देवें|
2. अमेरिकन और बीटी किस्मों में प्रति हैक्टेयर 75 किलोग्राम नत्रजन तथा 35 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है|
3. देशी किस्मों को प्रति हैक्टेयर 50 किलोग्राम नत्रजन और 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है|
4. पोटाश उर्वरक मिट्टी परीक्षण के आधार पर देवें, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई से पहले देवें| नत्रजन की शेष आधी मात्रा फूलों की कलियां बनते समय देवें|
सूक्ष्म तत्व सिफारिश- मिटटी जांच के आधार पर जिंक तत्व की कमी निर्धारित होने पर बुवाई से पूर्व बी टी या नरमा कपास में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी में मिलाकर बुरका दिया जाना चाहिए| यदि बुवाई के समय जिंक सल्फेट नही दिया गया हो तो 0.5 प्रतिशत जिंक सल्फेट के घोल का दो छिड़काव पुष्पन और टिण्डा वृद्धि अवस्था पर करने से अधिक पैदावार ली जा सकती है| इस उपचार से जड़ गलन की समस्या से भी निजात मिलेगी|
सल्फर- अमेरिकन कपास मे यदि फास्फोरस डी ए पी द्वारा देते हैं| तो उसके साथ 150 किलोग्राम जिप्सम प्रति हैक्टर देवें| यदि फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा दे रहे हो तो जिप्सम देने की आवश्यकता नहीं है|
यह भी पढ़ें- बीटी कॉटन की उन्नत किस्में, जानिए विशेषताएं एवं पैदावार
कपास फसल की सिंचाई प्रबंधन
1. बुवाई के बाद 5 से 6 सिंचाई करें, उर्वरक देने के बाद एवं फूल आते समय सिंचाई अवश्य करें| दो फसली क्षेत्र में 15 अक्टूबर के बाद सिंचाई नहीं करें|
2. अंकुरण के बाद पहली सिंचाई 20 से 30 दिन में कीजिये| इससे पौधों की जड़े ज्यादा गहराई तक बढ़ती है| इसी समय पौधों की छंटनी भी कर दीजिये| बाद की सिंचाईयां 20 से 25 दिन बाद करें|
3. नरमा या बी टी की प्रत्येक कतार में ड्रिप लाईन डालने की बजाय कतारों के जोड़े में ड्रिप लाईन डालने से ड्रिप लाईन का खर्च आधा होता है|
4. इसमें पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हुए जोडे में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और जोडे से जोडे की दूरी 120 सेंटीमीटर रखें| प्रत्येक जोडे में एक ड्रिप लाईन डाले तथा ड्रिप लाईन में ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर हो और प्रत्येक ड्रिपर से पानी रिसने की दर 2 लीटर प्रति घण्टा हो|
5. सूखे में बिजाई करने के बाद लगातार 5 दिन तक 2 घण्टे प्रति दिन के हिसाब से ड्रिप लाईन चला देवें| इससे उगाव अच्छा होता है और बुवाई के 15 दिन बाद बून्द-बून्द सिंचाई प्रारम्भ करें|
6. बून्द-बूंद सिंचाई का समय संकर नरमा की सारणी के अनुसार ही रखे, वर्षा होने पर वर्षा की मात्रा के अनुसार सिंचाई उचित समय के लिये बन्द कर दें| पानी एक दिन के अन्तराल पर लगावें|
7. 10 मीटर क्यारी की चौड़ाई और 97.50 प्रतिशत कट ऑफ रेशियो पर अधिकतम उपज ली जा सकती है|
8. बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से सिफारिश किये गयी नत्रजन की मात्रा 6 बराबर भागों में दो सप्ताह के अन्तराल पर ड्रिप संयंत्र द्वारा देने से सतही सिंचाई की तुलना में ज्यादा उपयुक्त पायी गयी है|
9. इस पद्धति से पैदावार बढ़ने के साथ-साथ सिंचाई जल की बचत, रूई की गुणवत्ता में बढ़ौतरी और कीड़ों के प्रकोप में भी कमी होती है|
किसान भाइयों को सिंचाई निचे सूचि के अनुसार एक दिन के अन्तराल पर बुवाई के दिन के बाद से शुरू कर देना चाहिए, जो इस प्रकार है, जैसे-
| महिना | घंटे | मिनट |
| मई | 2 | – |
| जून | 2 | 30 |
| जुलाई | 3 | – |
| अगस्त | 3 | 30 |
| सितम्बर | 2 | 20 |
| अक्तूबर | 1 | 30 |
यह भी पढ़ें- देसी कपास की उन्नत और संकर किस्में: विशेषताएं व पैदावार
कपास फसल की निराई-गुड़ाई
1. निराई-गुड़ाई सामान्यतः पहली सिंचाई के बाद बतर आने पर कसौले से करनी चाहिए| इसके बाद आवश्यकतानुसार एक या दो बार त्रिफाली चलायें|
2. रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेन्डीमेथालीन 30 ई सी, 833 मिलीलीटर (बीजों की बुवाई के बाद मगर अंकुरण से पहले) या ट्राइलूरालीन 48 ई सी, 780 मिलीलीटर (बीजाई से पूर्व मिट्टी पर छिड़काव) को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से लेट फेन नोजल से उपचार करने से फसल प्रारम्भिक अवस्था में खरपतवार विहीन रहती है| इनका प्रयोग बिजाई से पूर्व मिट्टी पर छिड़काव भली-भांति मिलाकर करें|
3. प्रथम सिंचाई के बाद कसोले से एक बार गुड़ाई करना लाभदायक रहता है| यदि फसल में बोई किस्म के अलावा दूसरी किस्म के पौधे मिले हुए दिखाई दें तो उन्हें निराई के समय उखाड़ दीजिए क्योंकि मिश्रित कपास का मूल्य कम मिलता है|
कपास के फूल और टिंडे कैसे रोकें
स्वतः गिरने वाली पुष्प कलियों और टिण्डों को बचाने के लिए एन ए ए 20 पी पी एम (2 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी) का घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियाँ बनते समय एवं दूसरा टिण्डों के बनना शुरू होते ही करना चाहिए|
कपास में डिफोलिएसन नियंत्रण
नरमा कपास की फसल में पूर्ण विकसित टिण्डे खिलाने हेतु 50 से 60 प्रतिशत टिण्डे खिलने पर 50 ग्राम ड्राप अल्ट्रा (थायाडायाजुरोन) को 150 लीटर पानी में घोल कर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करने के 15 दिन के अन्दर करीब-करीब पूर्ण विकसित सभी टिण्डे खिल जाते हैं| ड्राप अल्ट्रा का प्रयोग करने का उपयुक्त समय 20 अक्टूबर से 15 नवम्बर है| इसके प्रयोग से कपास की पैदावार में वृद्धि पाई गई है| गेहूं की बिजाई भी समय पर की जा सकती है|
जिन क्षेत्रों में कपास की फसल अधिक वानस्पतिक बढ़वार करती है, वहाँ पर फसल की अधिक बढ़वार रोकने के लिए बिजाई 90 दिन उपरान्त वृद्धि निपवण रसायन साईकोसिल 80 पी पी एम (8 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी) का छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- अमेरिकन कपास की उन्नत और संकर किस्में
कपास फसल में कीट नियंत्रण
कपास की फसल को वैसे तो बहुत सारे कीट हानि पहुंचाते हैं। परन्तु जो कीट आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं| उनके बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है, जैसे-
हरा तेला- पत्तियों की निचली सतह पर शिराओं के पास बैठकर रस चूस कर हानि पहुंचाता है, जिससे पत्तियों के किनारे हल्के पीले पड़ जाते हैं, फलस्वरूप ये पत्तियाँ किनारों से नीचे की तरफ मुड़ने लगती है|
नियंत्रण-
1. परभक्षी कीट क्राईसोपा 10 हजार प्रति बीघा की दर से छोड़े और आवश्यकता पड़ने पर परभक्षी को फूल अवस्था में पुनः दोहरायें|
2. प्रकोप अधिक होने पर निम्नलिखित रसायनों इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल, 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर या मोनोक्रोटोफास 36 एस एल, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या एसीफेट 75 एस पी, 2.0 ग्राम प्रति लीटर या डाइमिथोएट 30 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या थायोमिथोक्साम 25 डब्ल्यू जी, 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- कपास फसल की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार कीट और रोग
सफेद मक्खी- यह पत्तियों की निचली सतह से रस चूसती है और साथ ही शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जिसके ऊपर फहूँद उत्पन्न होकर बाद में पत्तियों को काला कर देती है| अधिक प्रकोप होने पर पत्तियाँ राख और तेलिया दिखाई देती है| यह कीट विषाणु रोग (पत्ता मरोड़क) भी फैलाता है|
नियंत्रण-
1. कीट रोधी बीकानेरी नरमा, मरू विकास, आर एस- 875 उगायें जैसी किस्में उगाएं|
2. 8 से 12 येलो स्टिकी ट्रेप प्रति बीघा की दर से फसल में कीट के सक्रिय काल में लगायें|
3. परभक्षी कीट क्राइसोपा 12 हजार प्रति बीघा की दर से छोड़े और आवश्यकता पड़ने पर परभक्षी को फूल अवस्था में पुनः दोहरायें|
4. अधिक प्रकोप होने पर ट्राइजोफास 40 ई सी, 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल, 0.3. मिलीलीटर प्रति लीटर या मिथाईल डिमेटोन 25 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या एसिटामिप्रीड 20 एस पी, 0.4 ग्राम प्रति लीटर या थायोक्लोप्रिड 240 एस सी,1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या थायोमिथोग्जाम 25 डब्ल्यू जी, 0.5 ग्राम प्रति लीटर या डाईफेन्थूरान 50 डब्ल्यू पी, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
चितकबरी सुंडी- प्रारम्भ में लटें तने और शाखाओं के शीर्षस्थ भाग में प्रवेश कर उन्हें खाकर नष्ट करती है, इससे कीट ग्रसित ये भाग सूख जाते हैं| लट से प्रभावित कलियों की पंखुड़ियाँ पीली होकर आपस में एक दूसरे से दूर हटती हुई दिखाई देती है। जैसे ही पौधों पर कलियाँ, फूल एवं टिण्डे बनने शुरू होते हैं लटें उन पर आक्रमण कर देती है|
नियंत्रण-
1. फसल में कीट ग्रसित तने और शाखाओं के शीर्षस्थ भागों को तोड़कर उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिये|
2. 5 से 10 फेरेमोन ट्रेप (लिंग आकर्षक) प्रति हैक्टेयर नर पतंगों का पता और उनको नष्ट करने हेतू लगाये|
3. परजीवी ट्राइकोग्रामा 40 हजार प्रति बीघा की दर से शाम के समय फसल में छोड़े| यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार (7 दिन अन्तराल) पर अवश्य दोहरायें|
4. परभक्षी कीट क्राईसोपा 12 हजार प्रति बीघा की दर से छोड़े| आवश्यकता पड़ने पर परभक्षी को फूल अवस्था में पुनः छोड़ें|
5. अधिक प्रकोप होने पर निम्नलिखित रसायनों मोनोक्रोटोफॉस 36 एस एल, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या फेनवेलरेट 20 ई सी, 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या मेलाथियॉन 50 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्लोरपाईरीफॉस 20 ई सी, 5.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई सी, 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्यूनालफॉस 25 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या इन्डोक्साकार्ब 14.5 एस सी, 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाईनोसेड 45 एस सी, 0.33 मिलीलीटर प्रति लीटर या फ्लूबेन्डियामाइड 480 एस सी, 0.40 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- कपास में एकीकृत कीट प्रबंधन कैसे करें
अमेरिकन सुंडी- पौधों में फलीय भाग उपलब्ध न होने पर पत्तियों को खाकर और गोल-गोल छेद कर नुकसान करती है| फूल एवं टिण्डों के अन्दर नुकसान करती हुई लटों का मल पदार्थ फल भागों के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। कीट का सक्रिय काल सामान्य तौर पर मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर परन्तु विशेष परिस्थिति में कीट का आक्रमण आगे-पीछे भी हो सकता है|
नियंत्रण-
1. प्रकाश पाश (लाईट ट्रेप) को सूर्य अस्त होने के दो घण्टे बाद तथा सूर्योदय के दो घण्टे पूर्व जलाकर प्रौढ़ पतंगों को आकर्षित कर नष्ट किया जा सकता है|
2. परजीवी ट्राइकोग्रामा 40 से 50 हजार प्रति बीघा की दर से फेरोमोन ट्रेप के अन्दर प्रौढ़ और फसल में अण्डे दिखाई देने पर ही छोड़े|
3. परभक्षी क्राइसोपा 10 से 12 हजार प्रति बीघा की दर से फसल में पत्तों पर अण्डे दिखाई देने पर छोड़ें|
4. न्युक्लियर पोलिहाइड्रोसिस वायरस (एन पी वी) का 0.75 मिली लीटर (एल ई) प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें|
5. नीम युक्त दवा (300 पीपीएम) 5.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़कें|
6. अधिक प्रकोप होने पर निम्नलिखित रसायनों क्यूनालफॉस 25 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या मेलाथियॉन 50 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई सी, 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या थायोडिकार्ब 75 एस पी, 1.75 ग्राम प्रति लीटर या इथियान 50 ई सी, 3.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या बीटासिफलूथिन 2.5 ई सी, 0.75 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्लोरपाईरीफॉस 20 ई सी, 5.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या अल्फामेथ्रिन 10 ई सी, 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- दीमक से विभिन्न फसलों को कैसे बचाएं
गुलाबी सुंडी- गुलाबी सुंडी के नुकसान की पहचान अपेक्षाकृत कठिन होती है, क्योंकि लटें फलीय भागों के अन्दर छुपकर एवं प्रकाश से दूर रहकर नुकसान करती है| फिर भी अगर कलियाँ फूल एवं टिण्डों को काटकर देखें तो छोटी अवस्था की लटें प्रायः फलीय भागों के ऊपरी हिस्सों में मिलती है|
नियंत्रण-
1. ऐसे सभी फूल जिनकी पंखुड़ियाँ ऊपर से चिपकी हो उन्हें हाथ से तोड़कर उनके अन्दर मौजूद गुलाबी सुंडियों को नष्ट किया जा सकता है| यह प्रक्रिया सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य करें|
2. 5 फेरोमोन ट्रेप प्रति हैक्टेयर नर पतंगों को नष्ट करने हेतु लगायें|
3. अधिक प्रकोप होने पर निम्नलिखित रसायनों साइपरमेथ्रिन 10 ई सी, 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 25 ई सी, 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर या कार्बरिल 50 डब्ल्यू पी, 4.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राइजोफॉस 40 ई सी, 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या मेलाथियॉन 50 ई सी, 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई सी, 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर या फ्लूबेन्डियामाइड 480 एस सी, 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
तम्बाकू लट- यह लट बहुत ही हानिकारक कीट है| इसकी लटें पौधों की पत्तियाँ खाकर जालीनुमा बना देती है व कभी-कभी पौधों को पत्तियाँ रहित कर देती है|
नियंत्रण-
1. इस कीट के अंण्डो के समूह जो कि पत्तियों की नीचे वाली सतह पर होते हैं उन्हें इकट्ठा करके नष्ट कर दें, लटों को हाथ से इक्ट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए|
2. प्रौढ़ कीट (पतंगों) को फेरोमोन ट्रेप लगाकर पकड़ा जा सकता है, इसलिए 10 ट्रेप प्रति हैक्टर की दर से खेत में लगाने चाहिए|
3. अधिक प्रकोप होने पर निम्नलिखित रसायनों थायोडिकार्ब 75 एस पी, 1.75 ग्राम प्रति लीटर या क्लोरपाइरिफास 20 ई सी, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्यूनालफॉस 25 ई सी, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या एसीफेट 75 एस पी, 2 ग्राम प्रति लीटर या न्यूवालूरोन 10 ई सी, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमामैक्टीन बैनजोएट 5 एस जी, 0.5 ग्राम प्रति लीटर या फलूबैन्डीयामाइड 480 एस सी, 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- कपास में समेकित नाशीजीव प्रबंधन कैसे करें
मीलीबग- इस कीट के मुखांग रस चूसने वाले होते है| कीट अनुकूल परिस्थितियों में भूमि से निकल कर खेत के आसपास के खरपतवारों पर संरक्षण लेते है| फिर मुख्य फसल पर आता है| खेत में अधिक प्रकोप होने पर ही पता चलता है| कीट के निम्फ या क्रावलर्स व व्यस्क दोनों ही पत्तियों, डण्ठलों, कलियों, फूलों, टहनियों व टिण्डों से रस चूसते है| कीट के अधिक प्रकोप से पत्तियाँ पीली हो कर गिर जाती हैं| तना सूख कर सिकुड़ जाता है व काला हो जाता है और फूल टिण्डे सूख कर गिर जाते है|
नियंत्रण-
1. फसल चक्र को अपनायें, एक ही खेत में लगातार कपास की फसल न लें|
2. मीलीबग की रोकथाम हेतु चीटियों का नियंत्रण करना जरूरी है|क्योंकि मीलीबग चीटिंयों की सहायता से एक खेत से दूसरे खेत में प्रवेश कर जाती है| इसके लिए खेत के चारों तरफ अवरोधक का घेरा बनायें तथा क्यूनालफॉस डस्ट का प्रयोग करें| चीटियों के बिलों को नष्ट कर दें|खेत में ग्रसित फसलों के अवषेशों को इकट्ठा करके जला दें और खेत के चारों तरफ उगे खरपतवारों को नष्ट कर दें|
3. मीलीबग कपास की छंटियों के अंदर रहते हैं अतः छुट्टियों को फरवरी माह से पहले-पहले जला देना चाहिए, छुट्टियों का खेत में ढेर नहीं लगाना चाहिए| 7. फसल के चारों तरफ बाजरा व ज्वार की दो-दो कतार में बोयें लेकिन फसल के पास ग्वार, भिण्डी को न बोयें|
जैव नियंत्रण-
मिलीबग कीट पर आक्रमण करने वाले कीट, जैसे-
परभक्षी- (लेडीबर्ड बीटल) बरूमेडस लिनीटस, कोक्सीनैला सेप्टमपंक्टेटा, चिलोमेन्स सेक्समाकूलाटा, रोडोलिया फूमिडा, क्रीप्टोलीम्स मोनट्रोज्यूरी व क्राइसोपरला कारनी परभक्षी कीटो को खेत में छोड़े|
परजीवी कीट- अनागीरस रामली व अनीसीअस बोम्बावाली भी खेत में छोड़ें|
रासायनिक नियत्रंण-
1. कीटनाशक रसायनों का छिड़काव पौधे के तने व ऊपरी भाग पर अच्छी तरह से करें व दूसरा छिड़काव जल्दी ही दोहरायें|
2. मीलीबग से ग्रसित खेत को तैयार करते समय क्यूनालफॉस धूडा 25 किलोग्राम प्रति हैक्टर की दर से मिला देवें या खेत में पलेवा देते समय क्लोरपाइरीफास 20 ई सी, 4 लीटर प्रति हैक्टर सिंचाई के साथ दें|
3. अधिक प्रकोप होने पर निम्नलिखित रसायनों का मिथाईल डिमेटोन 25 ई सी, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्यूनालफॉस 25 ई सी, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या ट्राईजोफॉस 40 ई सी, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या प्रोफेनोफास 50 ई सी, 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या एसिटामिप्रिड 20 एस पी, 1 ग्राम प्रति लीटर या क्लोरपाइरीफॉस 20 ई सी, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या एसीफेट 75 एस पी 2 ग्राम प्रति लीटर या थायोडीकार्ब 75 डब्ल्यू पी, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- कपास में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें
कपास फसल में रोग नियंत्रण
जीवाणु अंगमारी- इस रोग की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करते समय निम्न दवाओं को प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जैसे-
1. स्ट्रेप्टोसाईक्लिन- 5 से 10 ग्राम या प्लाटोमाइसीन या पोसामाइसीन – 50 से 100 ग्राम
2. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड – 300 ग्राम|
जड़गलन- जड़गलन की समस्या वाले खेतों में बुवाई से पूर्व बोये जाने वाले बीजों को कार्बोक्सिन 70 डब्ल्यू पी, 0.3 प्रतिशत या कार्बेन्डेजिम 50 डब्ल्यू पी, 0.2 प्रतिशत 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में भिगोकर, भिगोये गये बीज को कुछ समय तक छाया में सुखाने के बाद ट्राइकोडर्मा हरजेनियम जीव या सूडोमोनास फ्लूरोसेन्स 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोये|
जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक है उन खेतों के लिए बुवाई के पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हरजेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद (एफ वाई एम) में अच्छी तरह मिलाकर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में रख दें|
इस मिश्रण को बुवाई के समय डेढ़ बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें, साथ में ट्राइकोडरमा जैव से बीज उपचार करें| रोग ग्रस्त खेतों में कपास और मोठ की मिश्रित फसल लीजिए| रोग का प्रकोप अधिक हो तो रोगग्रस्त खेतों में दो वर्ष तक कपास की फसल न लेंवे|
कपास की चुनाई कब करें
कपास में टिंडे पूरे खिल जाये तब उनकी चुनाई कर लीजिये| प्रथम चुनाई 50 से 60 प्रतिशत टिण्डे खिलने पर शुरू करें और दूसरी शेष टिण्डों के खिलने पर करें|
कपास की फसल से पैदावार
उपरोक्त उन्नत विधि से खेती करने पर देशी कपास की 20 से 25, संकर कपास की 25 से 32 और बी टी कपास की 30 से 50 क्विण्टल प्रति हैक्टेयर पैदावार ली जा सकती है|
यह भी पढ़ें- कपास में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें: उत्तम उत्पादन हेतु
अगर आपको यह लेख पसंद आया है, तो कृपया वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें| आप हमारे साथ Twitter और Facebook के द्वारा भी जुड़ सकते हैं|
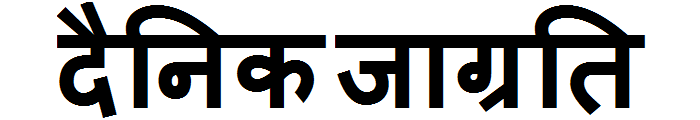
प्रातिक्रिया दे