
जौ के प्रमुख कीट और रोकथाम जौ घास परिवार में रबी फसल के रूप में उगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनाज हैं तथा इसे भारत के उत्तर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता हैं| वर्तमान में जौ दुनिया में चौथे स्थान पर (गेहूं, चावल और मक्का के बाद) उगाई जाने वाली औषधीय और पौष्टिक अनाज हैं| परन्तु हम जौ की पैदावार में अन्य देशों से काफी पिछड़े है| भारत में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है|
हमारे देश में जौ का उपयोग भोजन, पशुओं का चारा, माल्ट और माल्ट सत्व से विभिन्न प्रकार के बीयर, हिस्की मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिये किया जाता है| औषधीय और पौष्टिक विशेषताओं के कारण जौ का भोज्य पदार्थों में उपयोग बढ़ रहा है| इसे बेबी फूड्स, पेय, औषधीय सिरप, शरीर का रक्तचाप, तापमान और सूगर कम करने हेतु उपयोग होता है|
किसान इसे कम पानी उपलब्ध क्षेत्र में, हलकी भूमि, सीमांत भूमि और लवणीय या क्षारीय भूमि क्षेत्र में भी उगाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं| यह फसल देश के दक्षिणी राज्यों में बहुत कम क्षेत्र पर उगाई जाती है, फिर भी अब वहाँ के किसान जौ को उगाना पसन्द कर रहे हैं तथा इसके बढ़ते हुये उपयोग के कारण यह बहुत जरूरी भी है|
यह भी पढ़ें- गेहूं एवं जौ में सूत्रकृमि प्रबंधन
देश में जौ का उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसन्धान चल रहा है| हर साल ज्यादा उपज देने वाली प्रजातियाँ तैयार की जा रही हैं| जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जौ के बीज पर छिलका होता है, जो उसके उपयोग में बाधा डालता है| लेकिन अब छिलका रहित प्रजातियाँ जैसे- करन 16, करन 19, करन 521, एन डी बी- 10, गीतांजलि उपलब्ध होने के कारण उसे भोजन में उपयोग करना सरल हो गया हैं|
लेकिन जैविक तथा अजैविक तनावों का प्रतिरोध करने वाली प्रजातियाँ तैयार करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे फसल उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है| किसान जौ के कीटों का रोकथाम करके भी उपज बढ़ा सकते हैं, इस लेख में इसका उल्लेख है| यदि जौ की खेती की पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें- जौ की खेती की जानकारी
जौ के कीटों की रोकथाम
माहू कीट
लक्षण- जौ के कीटों में माहू जौ की पूरी पत्ती पर पाई जाती है, इसके मल के कारण पत्ती पर चिपचिपाहट पैदा होती है| माहू अपने मुँह का उपयोग करके पत्तियों से रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देता है| पत्तियों झुलसकर सूखने लगती हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं| कमजोर पौधे में कभी-कभी तो बालियाँ नहीं निकलती या निकलती भी हैं, तो उसमें दोनों का भराव कम होता है| जो दाने भरते भी हैं, वे इतने पतले होते हैं कि उनका वजन नगण्य होता है|
इसके कारण जौ के उत्पादन पर भारी असर पड़ता हैं| आमतौर पर इसका प्रकोप जनवरी महीने में जब कुण्ड बढ़ने लगती हैं, तब बहुत ज्यादा हो जाता है| किसान जितनी देर से बुवाई करता है, माहू का प्रकोप उतना ज्यादा होता है| अगर जौं में बाली निकलने से पहले, एक पत्तीं पर 50 से ज्यादा माहू पाये जाते हैं तो हमें रोकथाम के उपाय करना जरूरी हैं|
रोकथाम-
1. अगर जौ की बुवाई समय पर हो जाये, तो इस कीट का प्रकोप काफी औसत में कम हो जाता है|
2. यदि शुरू में कीट जौ के क्षेत्र में दिखने लगे तो, उन पत्तियों को तोड़कर जला देना चाहिये, ताकि उनका फैलाव दूसरे पौधों पर ना हो|
3. नत्रजन खादों के अधिक उपयोग के कारण माहू का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिये किसान को नत्रजन खादों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिये|
4. अगर लेडी बग बीटल जैसे परभक्षी मित्र कीट पौधों पर दिखने लगे तो, हमें नीम अर्क, 5 प्रतिशत यानी 10 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर अर्क का इस्तेमाल करना चाहिये|
5. यदि माहू कि संख्या एक पत्तों पर 50 से ज्यादा पाई जाती है तो मैलाथियान 50 ई सी का या डाईमेथोएट 30 ई सी या मेटासिस्टॉक्स 25 ई सी का 15 से 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये|
यह भी पढ़ें- जौ के प्रमुख रोग एवं रोकथाम
दीमक
लक्षण- इसके प्रकोप से जौ के पौधे सूखने लगते है तथा हाथ से खिचने के बाद जड़ से निकल जाता है| इसका प्रकोप फसल की सम्पूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है| यह जमीन में रहकर जड़ को खा जाता है, जिसके कारण जौ के पौधे सुखकर मर जाते हैं| सामाजिक कीट होने के कारण यह आसानी से पहचाना जा सकता है| अविघटित जैविक खाद का उपयोग करने से भी दीमक की भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी हो जाती है तथा किसान को जौ के उत्पादन में भारी नुकसान होता है|
रोकथाम-
1. हमेशा खूब सड़ी जैविक खाद का ही खेत में उपयोग करना चाहिये|
2. बीज को बुवाई से 2 से 3 दिन पूर्व इमिडाक्लोरोप्रीड 70 डब्ल्यू एस 0.1 प्रतिशत प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिये|
3. आवश्यकता होने पर क्लोरोपायरीफॉस 20 ई सी, 3.5 लीटर प्रति हेक्टर इस्तेमाल करना चाहिये|
4. खेत के 80 मीटर दायरे में यदि इसकी वांबी हो तो उसे ढूंढ कर समूल नष्ट कर देना चाहिये|
5. चीटियाँ या लाल चीटें इनके स्वाभाविक दुश्मन होते हैं इनको गुड या चीनी या अन्य किसी माध्यम से इनकी वॉबी तक पहुँचा कर इनको नष्ट किया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- सस्य क्रियाओं द्वारा कीट नियंत्रण
सैनिक कीट
लक्षण- यह भी एक हानिकारक कीट है, इसकी लम्बाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है| उसकी नवजात सूडी शुरू में पौधे के मध्य वाली कोमल पत्तियों को खाती हैं| जैसे-जैसे सुंडी प्रौढ़ होने लगती है, वैसे-वैसे इसका रंग भूरा होने लगता है| यह कीट शाम के समय पौधों पर पत्तियाँ खाते दिखता है|
दिन भर यह जमीन की दरारों में छिपा रहता है| जब सैनिक कीट का प्रकोप बहुत बढ़ता है, तो यह पौधे कि सारी पत्तियाँ खा जाता है, बस मुख्य शिरा बच जाता है| कभी-कभी यह कीट जौ के अपरिपक्व दानें भी खा जाता हैं|
रोकथाम-
1. यह कीट जमीन में और पिछले फसल के अवशिष्टों में सुप्त हालत में पड़ा रहता है, इसलिये हमें फसल की बुवाई से पूर्व खेत में से इन अवशिष्टों को नष्ट कर देना चाहिये|
2. फसल में से खरपतवार निकालकर नष्ट करने से भी इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है|
3. इस कीट का ज्यादा प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 ई सी 15 से 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये|
यह भी पढ़ें- समेकित कृषि प्रणाली क्या है, इससे कैसे बढ़ सकती है किसानों की आय
प्रिय पाठ्कों से अनुरोध है, की यदि वे उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|
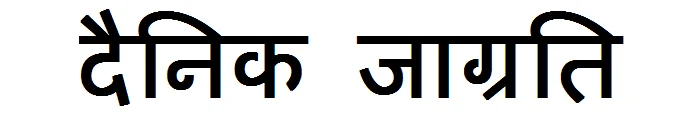
Leave a Reply