
मूंग और उड़द भारत की महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं| इनके के उत्पादन में हमारा देश विश्व का अग्रणी है| विभिन्न फसलों के साथ और फसल-चकों में उगाये जाने के कारण दलहनी फसलों में मूंग और उड़द का प्रमुख स्थान है| हमारे देश में इसकी खेती दलहनी फसलों के लगभग 30 प्रतिशत भाग में विभिन्न ऋतुओं में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्रतल से 1820 मीटर की ऊँचाई तक होती है|
भारत में मूंग और उड़द की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर (मूंग 29.8 एवं उड़द 29.7 लाख हेक्टेयर) में की जाती है और उत्पादन 26 लाख टन (मूंग 12.6 एवं उड़द 13.3 लाख टन) और उत्पादकता कमशः 353 से 447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है| क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र पहला स्थान पर और उत्पादकता के अनुसार मूंग में पंजाब 622 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उड़द में बिहार 824 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ पहले स्थान पर है|
रोग एंव प्रबंधन मूंग और उड़द की फसल विभिन्न विषाणुओं, कवकों व जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों से प्रभावित होती है| यदि इन रोगों की सही पहचान करके ठीक समय पर प्रबंधन कर लिया जाये, तो पैदावार का काफी भाग ह्रास से बचाया जा सकता है| इस लेख में मूंग और उड़द की फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग एंव उनका समेकित प्रबंधन का उल्लेख है|
मूंग की उन्नत खेती की पूरी जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- मूंग की खेती- किस्में, रोकथाम व पैदावार
उड़द की उन्नत खेती की पूरी जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- उड़द की खेती- किस्में, रोकथाम व पैदावार
मूंग और उड़द की फसलों के रोगों का प्रबंधन
सरकोरस्पोरा पत्र बुंदकी रोग
मूंग और उड़द का यह एक प्रमुख रोग है, जिससे प्रतिवर्ष पैदावार में भारी क्षति होती है| यह रोग भारत के लगभग सभी मूंग और उड़द उगाने वाले क्षेत्रों में व्यापकता से पाया जाता है| जब वातावरण में नमीं अधिक होती है, तो यह रोग उग्र रुप में प्रकट होता है और अनुकूल वातावरण में यह रोग एक महामारी का रुप ले लेता है|
लक्षण-
1. सरस्कोस्पोरा पत्र बुंदकी रोग के कारण पत्तियों पर भूरे गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिनका बाहरी किनारा भूरे लाल रंग का होता है| यह धब्बे पत्ती के ऊपरी हिस्से पर अधिक स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं|
2. संक्रमण पुरानी पत्तियों से प्रारम्भ होता है|
3. अनुकूल परिस्थतियों में यह धब्बे बड़े आकार के हो जाते हैं तथा अन्ततः पुश्पीकरण फलियाँ बनते समय रोग ग्रसित पत्तियाँ गिर जाती हैं|
4. सामान्यतः पुरानी फलियों में ही संक्रमण होता है जो कि अधिक धब्बे बनने की स्थिति में काली पड़ जाती हैं और ऐसी फलियों में दाने भी बदरंग तथा सिकुड़ जाते हैं|
प्रबंधन-
1. बुबाई से पहले कैप्टन या थिरम कवकनाशी से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए|
2. फसल पर रोग के लक्षण दिखते ही कार्बेन्डाजिम 0.05 प्रतिशत या मेंन्कोजेब 6.2 प्रतिशत कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिएं, इसके पश्चात् आवश्यकतानुसार 1 से 2 छिड़काव 10 से 15 दिन के अन्तर पर करना चाहिए|
यह भी पढ़ें- मूंग में एकीकृत कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें
पीला चितेरी रोग
यह एक विषाणु जनित रोग है और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में व्यापक रुप से क्षति पहुंचाता है| यह रोग कई दलहनी फसलों व जंगली पौधों की कुछ किस्मों पर भी पाया जाता है| इस रोग का प्रकोप मूंग और उड़द में अधिक व्यापक होता है|
यह रोग मूंग और उड़द के अलावा अरहर, लोबिया और सोयाबीन में भी संक्रमण करता है| यह रोग सामान्य अवस्था में फसल बोने के लगभग दो सप्ताह के अन्दर प्रकट हो जाता है| इस रोग द्वारा पैदावार में कमी फसल के संक्रमित होने की अवस्था पर निर्भर करती है| रोग-ग्राही किस्मों में यदि रोग आरम्भिक अवस्था में होता है, तो उपज पैदावार भी हो सकती है|
लक्षण-
1. पीला चितेरी रोग के प्रारंभिक लक्षण पत्तियों पर पीले धब्बे के रुप में दिखायी पड़ते हैं| यह धब्बे एक साथ मिलकर तेजी से फैलते हैं, जिससे पत्तियों पर बड़े-बड़े पीले धब्बे बन जाते हैं| अंत में पत्तियाँ पूर्ण रुप से पीली हो जाती हैं|
2. पीली पत्तियों पर ऊतक क्षय भी देखा गया है|
3. रोग ग्रसित पौधे देर से परिपक्व होते है और पौधों में फूल तथा फलियॉ स्वस्थ्य पौधों की अपेक्षा बहुत ही कम लगती हैं|
4. पीला चितेरी रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियों के साथ-साथ फलियों और दानों पर पीले धब्बे देखे गये है|
यह भी पढ़ें- मूंग की उन्नत किस्में, जानिए उनकी विशेषताएं एवं पैदावार
रोग जनक एवं संचरण- मूंग और उड़द का यह रोग पीली चितेरी विषाणु द्वारा होता है| यह विषाणु मिटटी, बीज और संस्पर्श द्वारा संचारित नहीं होता है| पीली चितेरी रोग सफेद मक्खी ‘बेमिसिया टैबेकाइ, जो चूसक कीट है, के द्वारा फैलता है| सफेद मक्खी एक छोटी और कोमल काय मक्खी है| यह लगभग 0.5 से 1.0 मिलीमीटर तक लम्बी होती है| इसके शरीर का रंग बहुत हल्का पीला और पंखों का रंग सफेद होता है| सफेद मक्खी, जब एक स्वस्थ पौधे पर चूसण करती है, तो साथ में विषाणु का भी स्वस्थ पौधे में संचारण करती है| यही प्रक्रिया पूरे खेत में चलती है तथा रोग फैलता है|
रोग का चक्र- इस विषाणु की रोग वाहक कीट, सफेद मक्खी पूरे वर्ष किसी न किसी पादप जाति पर पाई जाती है| यह मक्खी अरहर से भी शरण करती है| गर्मियों में सफेद मक्खी अरहर से पीली चितेरी विषाणु ग्रहण करके ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द में विषाणु का संचारण करती है| ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के रोगी पौधे, वर्षाकालीन खरीफ मूग व उर्द की फसलों लिये इस विषाणु के निवेश द्रव्य के स्त्रोत का कार्य करते है| इस प्रकार पीली चितेरी विषाणु एक मौसम से दूसरे मौसम तक जीवित रहकर एक फसल से दूसरी फसल में फैलता रहता है| रोग फैलने की गति सफेद मक्खी की संख्या पर निर्भर करती है|
प्रबंधन-
1. यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है, इसलिये सफेद मक्खी का नियंत्रण करके इस रोग को नियन्त्रिण में किया जा सकता है| खेत में रोग दिखते ही आक्सीडेमेटान मेथाइल 0.1 प्रतिशत या डायमेथोएट 0.3 प्रतिशत प्रति हेक्टेअर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें| कुल मिलाकर 3 से 4 छिड़काव करने से रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है|
2. कुछ खरपतवार भी मूंग के पीली चितेरी रोग के विषाणु से संक्रमित होते हैं इसलिये खेत की निराई करके खरपतवार निकालते रहना चाहिये|
3. रोग ग्रसित पौधों को शुरु में ही उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए|
4. इस रोग का सबसे सरल और सस्ता उपाय मूंग और उड़द की चितेरी रोधी किस्मों का उगाना है| मूंग और उड़द की पीली चितेरी रोधी किस्में इस प्रकार है, जैसे-
मुंग- पन्त मूंग- 2, पन्त मूंग- 3, पन्त मूंग- 4, पूसा- 105, एम यू एम- 2, एम एल- 131, एम.एल- 267, एम एल- 337, नरेंद मुंग- 1, पी डी एम- 11 (बसंत ऋतु), पी डी एम- 84-139 (सम्राट) आदि|
उड़द- पन्त यू- 19, पन्त यू- 30, पी डी एम- 1 (बसंत ऋतु), यू जी- 218, पी एस- 1, नरेंन्द्र उड़द- 1, डब्लू बी यू- 108, डी पी यू- 88-31, आई पी यू- 94-1 (उत्तरा) आदि|
यह भी पढ़ें- अरहर की खेती- किस्में, रोकथाम और पैदावार
पर्ण व्यांकुचन रोग/झुर्रीदार पत्ती रोग
पर्ण व्याकुंचन मूंग और उड़द का एक अन्य मुख्य विषाणु रोग है| इस रोग को अधिकतर उड़द में ही देखा गया है| परन्तु मूंग भी संक्रमित होती है| इस विषाणु द्वारा पौधा अपनी प्रारम्भिक अवस्था में संक्रमित हो तो शत प्रतिशत हानि भी हो सकती है| इस रोग का प्रकोप दक्षिण भारतीय प्रदेशों के मूंग और उड़द उगाने वाले कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है|
लक्षण- इस रोग के लक्षण आमतौर पर फसल बोने के तीन से चार सप्ताह बाद प्रकट हो जाते हैं| इस रोग के विशिष्ट लक्षण पत्तियों की सामान्यता से अधिक वृद्धि और बाद में इनमें सिलवटें (झुर्रियां) या मरोड़पन होना है| ये पत्तियां छूने पर सामान्य पत्ती से अधिक मोटी एवं खुरदरी प्रतीत होती हैं| रोग जनक और संचरण- पर्ण व्यांकुचन एक विषाणु के द्वारा होता है|
प्रबंधन-
1. यह विषाणु रोगी पौधे के बीजों द्वारा संचारित होता है| इसलिये रोगी पौधों को शुरु में ही उखाड़कर जला देना चाहिये|
2. ऐसे क्षेत्र में जहां इस रोग का प्रकोप अधिक हो उड़द की पर्ण व्यांकुचन अवरोधी प्रजाति ए डी टी- 3 को उगाना चाहिए|
3. कीटनाशी के छिड़काव द्वारा भी इस रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- बीटी कपास (कॉटन) की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल एवं पैदावार
चूर्णी कवक
गर्म या शुष्क वातावरण में यह रोग जल्दी फैलता है| मध्य भारत और दक्षिणी प्रदेशों में यह व्यापकता से पाया जाता है|
लक्षण- इस रोग के मुख्य लक्षण पौधे के सभी वायवीय भागों में देखे जा सकते हैं| रोगों का संक्रमण सर्वप्रथम निचली पत्तियो पर कुछ गहरे धब्बों के रुप में प्रकट होते है| इन्ही धब्बों पर छोटे छोटे सफेद बिन्दु पड़ जाते हैं, जो बाद में बढ़ कर एक बड़ा सफेद धब्बा बनाते हैं| जैसे-जैसे रोग की उग्रता बढ़ती है, यह सफेद धब्बे आकार में बढ़ते हैं|
प्रबंधन-
1. उड़द की रोग अवरोधी किस्में जैसे- एल बी जी- 17, एल बी जी- 402 तथा मूंग की रोग रोधी किस्में जैसे- टी ए आर एम- 1, पूसा- 9072 इसमें उपयुक्त हैं|
2. फसल पर घुलनशील गंधक 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए|
3. फसल पर कार्बेन्डाजिम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या केराथेन कवकनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़कने से इस रोग का नियंत्रण हो जाता है, प्रथम छिड़काव रोग के लक्षण दिखते ही और आवश्यकतानुसार 2 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए|
यह भी पढ़ें- मूंग की बसंतकालीन उन्नत खेती कैसे करें
मोजेक मोटल रोग
यह रोग मूंग की अपेक्षा उड़द पर अधिक व्यापकता से होता है| इस रोग द्वारा पैदावार में कमीं पौधों के संक्रमित होने की अवस्था पर निर्भर करती है| प्रचण्ड संक्रमण द्वारा पौधे की पैदावार क्षमता शून्य ही जाती है, जिसके फलस्वरुप ऐसे पौधों की पैदावार में शत प्रतिशत हानि होती है|
लक्षण- इस रोग के प्रारम्भिक लक्षण पत्तियों पर प्रकट होते हैं| पत्तियां विकृत हो जाती हैं, बाद में पत्तियां सिकूड सी जाती हैं| संक्रमित पत्तियों पर फफोले पड़ जाते हैं तथा पौधों की वृद्धि सामान्य से कम होती हैं|
रोग जनक एवं संचरण- यह रोग बीज सामान्य मोजेक विषाणु के विभिन्न विभेदों द्वारा होता है| इस वायरस के कण नम्य छड़ रुप होते हैं| इनका जीनोम एक लड़ीय आर एन ए का बना होता है| यह विषाणु आमतौर पर दलहनी फसलों तक ही सीमित रहता है| यह विषाणु, बीज द्वारा संचारित होता है| संक्रमित बीजों से उत्पन्न पौधे संक्रमित होते हैं और यह पौधे विषाणु के प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं|
प्रबंधन
1. केवल प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए|
2. रोगी पौधों से प्राप्त बीजों को बोने लिये प्रयोग नहीं करना चाहिए|
3. रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए|
4. खेत में खरपतवार का उचित नियंत्रण करें|
5. कीटनाशी का छिड़काव करने से रोग वाहक कीटों का नियंत्रण करके भी एक सीमा तक इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- कपास की खेती कैसे करें
पर्ण संकुचन
मूंग और उड़द में पर्ण कुंचन रोग दक्षिणी प्रदेशों में मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश में यह रोग मूंग और उड़द की फसलों को बड़े स्तर पर हानि कर रहा है और प्रचण्ड रुप धारण करता प्रतीत होता है| उत्तर भारत में इस रोग का प्रकोप अधिक नहीं है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इसके प्रकोप में कुछ वृद्धि आयी है| इस रोग को पीली चितेरी रोग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण विषाणु रोग कहा जा सकता है|
लक्षण-
1. इस रोग के लक्षण पौधे पर प्रारम्भिक अवस्था से लेकर अन्तिम अवस्था तक किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं| प्रथम लक्षण सामान्यतः तरुण पत्तियों के किनारे पर पाश्र्व शिराओं और उसकी शाखाओं के चारो और हरिमहीनता का प्रकट होना है|
2. संक्रमित पत्तियों के सिरे नीचे की ओर कुंचित हो जाते है और यह भंगुर हो जाती हैं| ऐसी पत्तियों को यदि उंगली द्वारा थोड़ा सा झटका दिया जाए, तो यह डंठल सहित नीचे गिर जाती हैं|
3. संक्रमित पत्तियो की निचली सतह पर शिराओं में भूरे रंग का विवरण प्रकट हो जाता है जो कि डंठल तक में फैल जाता है| संक्रमित पौधों की वृद्धि रुक जाती है| यह पौधे खेत में अन्य पौधों की तुलना में बौने से दिखते हैं तथा इस कारण खेत में दूर से ही पहचाने जा सकते हैं|
यह भी पढ़ें- धान (चावल) की खेती कैसे करें
रोग जनक और संरक्षण- पिछले कुछ वर्षों तक इस रोग का जनक, टमाटर स्पाटिड विल्ट विषाणु के नाम से जाना जाता था, परन्तु अभी कुछ समय पहले यह ज्ञात हुआ है, कि यह रोग एक अन्य विषाणु जिसे ‘पीनट बड नेकासिस वाइस’ कहते हैं, के द्वारा होता है| यह रोग थ्रिप्स कीट की एक जाति द्वारा फैलता है| इस कीट का आकार बहुत छोटा होता है| यह पौधों के शीर्षस्थ भाग या पुष्प कलिकाओं या पुष्पों के अन्दर रहता है|
प्रबंधन- इस रोग के रोकथाम के बारे में शोध कार्य जारी है| अभी तक हुए शोध कार्यों के आधार पर बीजों को कीटनाशी इमिडाक्रोपिरिड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार और बुबाई के 15 दिन उपरान्त इसी कीटनाशी से छिड़काव 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर से इस रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है|
उपरोक्त का सार
मूंग और उड़द का भारत में शाकाहारी जनसंख्या के आहार में प्रोटीन का मुख्य स्त्रोत दालें हैं| प्रोटीन के अतिरिक्त इनमें खनिज लवण और अनेक विटामिन्स भी पाये जाते हैं| मूंग और उड़द की फसल कई प्रकार के हानिकारक रोगों द्वारा प्रभावित होती है| अगर इनका समय रहते नियंत्रण न किया गया तो बाजार मूल्य में गिरावट और अत्यधिक कृषकों को हानि का सामना करना पढ़ सकता है| इसलिए मूंग और उड़द के रोगों की पहचान और उनका प्रबंधन करना अत्यन्त आवश्यक है|
यह भी पढ़ें- अरहर में कीट एवं रोग नियंत्रण कैसे करें
यदि उपरोक्त जानकारी से हमारे प्रिय पाठक संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter व Google+ को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|
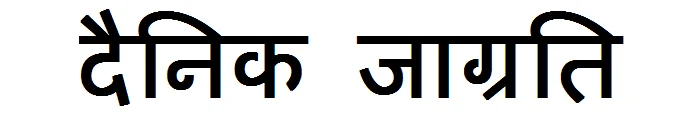
Leave a Reply